समझ नहीं आता , कभी पीएचडी अनिवार्य कर देते हैं कभी हटा देते हैं
पहले अनिवार्य नहीं थी तो क्यों की ?
जरूरी थी तो अब हटा क्यों दी ?
दरअसल अन्य कलाओं की तरह शोध भी एक कला है । जो सबके बस की बात नहीं है । संगीत पर लेक्चर देना एक अलग बात है और गीत गाना एक अलग बात है ।
शोध अनिवार्य नहीं था तो वही करता था जिसे बहुत तड़फ होती थी कुछ नया खोजने करने की । शोध की गुणवत्ता भी कायम रहती थी ।
फिर जब शोध अनिवार्य हुआ तो भीड़ बढ़ गई । शोध लिखने,लिखवाने और शोध पत्र छपवाने वालों की दुकानें खुल गई । शोध का स्तर गिरने लगा ।
जो पारंपरिक वास्तविक विद्वत्ता पूर्ण शोध जनरल थे ,वे ISSN आदि ,peer reveiw , UGC care listed आदि के कृत्रिम मानदंड पूरे न करने से बाहर हो गए और बाजारू प्रकाशकों ने मात्र जुगाड़ से इन नियमों की पूर्ति करके खुद को केअर लिस्ट में डलवा कर प्रामाणिक का लाइसेंस बनवा लिया और पैसा ले लेकर शोध पत्र छापकर विदयार्थियों की पीएचडी और अध्यापकों की प्रोन्नति करने लगे ।
शोध की चोरी पकड़ने मशीनें लगाई गईं तो उसमें भी असली शोध वाले फंस गए और नकली वाले तकनीकी जुगाड़ से निकल गए ।
छह महीने के कोर्स वर्क की बाध्यता अच्छे प्रशिक्षण के लिए की गई थी लेकिन उस एक माह के लायक विषय को जबरजस्ती छह माह तक पढ़ाना शोधार्थी का समय खराब करने से ज्यादा कुछ नहीं लगा ।
इन सब बाध्यताओं को सरकारी विश्वविद्यालय तो पालते रहते हैं लेकिन कोचिंग की तरह खुल रहे प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने फीस का पैसा कमाने के लिए इनके भी तोड़ निकाल लिए ।
शोध में एक होता है मौखिक परीक्षा का नाटक ,जो कब एक खाओ पीओ की पार्टी में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता । अन्य परीक्षाओं की तरह यह भी गोपनीय होना चाहिये तो उसका भी ढिंढोरा इस तरह पीटा जाता है मानो कोई बारात निकालनी हो ।
अकादमिक गंभीरता का नाश स्वयं नियम उपनियम बनाने वाले करते हैं ।
इसी के साथ साथ नियंता यदि वास्तव में शोध में गुणात्मक सुधार लाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है -
1. किसी भी विश्वविद्यालय में शोध को लेकर भाषात्मक बाध्यताएं न हों ,मसलन कई विश्वविद्यालय मात्र अंग्रेजी में ही शोध की अनुमति देते हैं यदि कोई हिंदी में लिखना चाहे तो अनुमति नहीं है ।
2. शोध की मूल्यांकन प्रक्रिया में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए । जैसे शोध प्रबंध का मूल्यांकन साधारण स्पाइरल बॉन्डिंग में ही हो और उसमें आरम्भ में शीर्षक ,विश्वविद्यालय के नाम के अलावा निर्देशक और शोधकर्ता का नाम ,धन्यवाद ज्ञापन आदि न हों ,यहां तक कि विभाग का नाम भी न हो । यह सब मौखिक परीक्षा के अनंतर हार्ड बांड में सभी औपचारिकताएं पूरी करके शोध प्रबंध जमा हो ।
3.शोध में मूल्यांकन हेतु मात्र विषय सूची और अध्याय ,डेटा,संदर्भ आदि अति आवश्यक चीजें ही भेजी जाएं ।
4. वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि मौखिक परीक्षा का प्रावधान खत्म ही कर दिया जाय । जिससे अनावश्यक विलंब और खर्चा बचे । क्यों कि मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कोई भी नहीं होता तो वह महज एक औपचारिकता ही है । इसके स्थान पर एक परीक्षक अतिरिक्त बढ़ा दिया जाय ।
5.शोध हेतु प्रवेश परीक्षा का आधार मात्र बहु विकल्पीय प्रश्नों के समाधान न हों । निबंधात्मक और शोधपरक प्रश्नों के उत्तर लिखने को भी कहा जाय ताकि उसकी शोध कला का मूल्यांकन हो सके ।
अन्यथा जिसने जीवन में एक शोध पत्र भी नहीं लिखा वह प्रवेश परीक्षा में चार में से एक विकल्प पर टिक करके प्रवेश पा जाता है और उससे शोध रूपरेखा तक लिखते नहीं बनती , शोध प्रबंध तो बहुत दूर ।
इसी तरह अकेला NET एक लेक्चरर की पात्रता जांचने के लिए काफी नहीं है । Bed की तरह महाविद्यालय ,विश्वविद्यालय आदि में पढ़ाने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए ।
जिस तरह शोध एक कला है उसी तरह अध्यापन भी एक कला और कौशल है । NET से ज्यादा से ज्यादा आप उनकी बुद्धि का ही यत्किंचित परीक्षण कर पाते हैं । विश्वविद्यालय में 150 वयस्क छात्रों को संबोधित करना और उन्हें व्याख्यान देना - हर ज्ञानी व्यक्ति के वश का नहीं होता है । उसका प्रशिक्षण भी जरूरी है यदि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार चाहिए । अन्यथा कई बार विषय के बहुत ज्ञानी और NET उत्तीर्ण शिक्षक भी कक्षा आदि ढंग से लेने में असमर्थ रहते हैं ।
continue ........
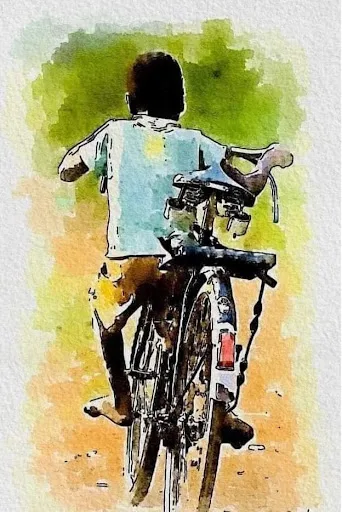
टिप्पणियाँ